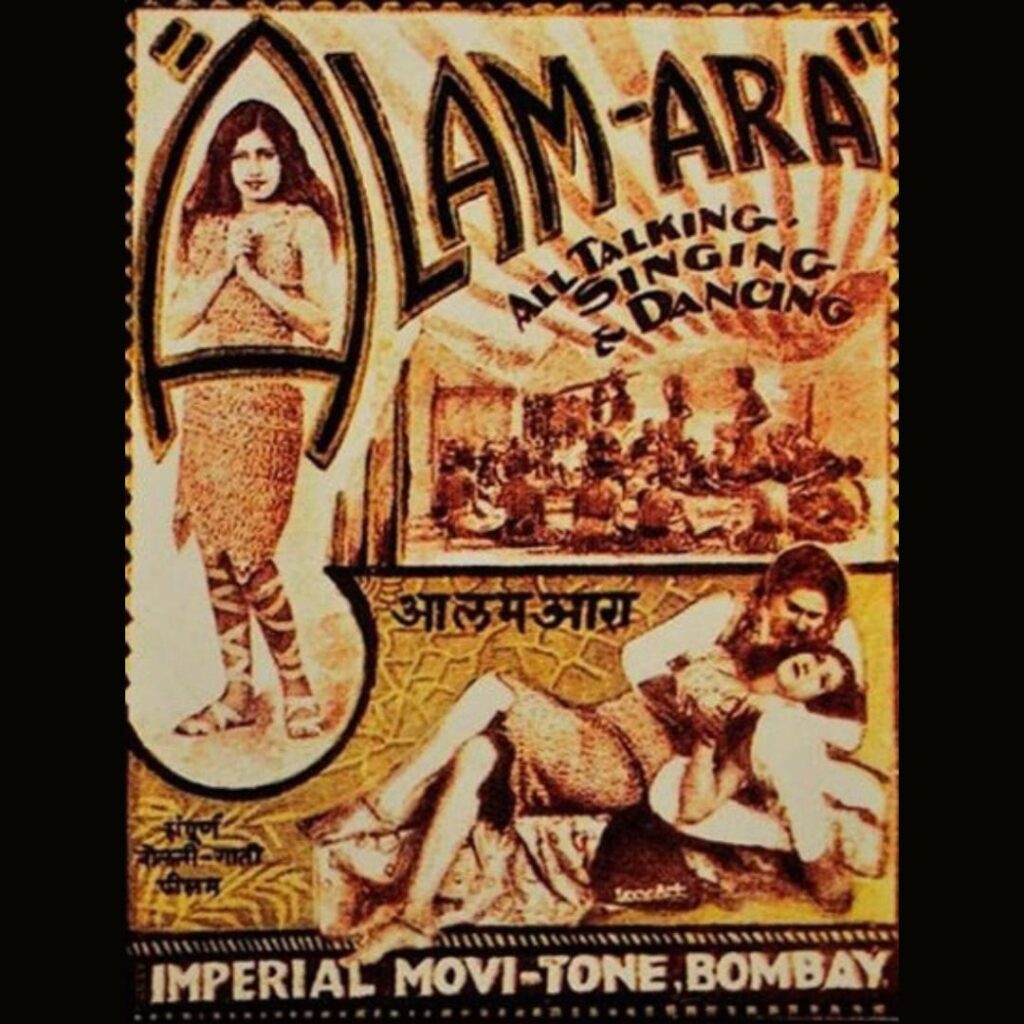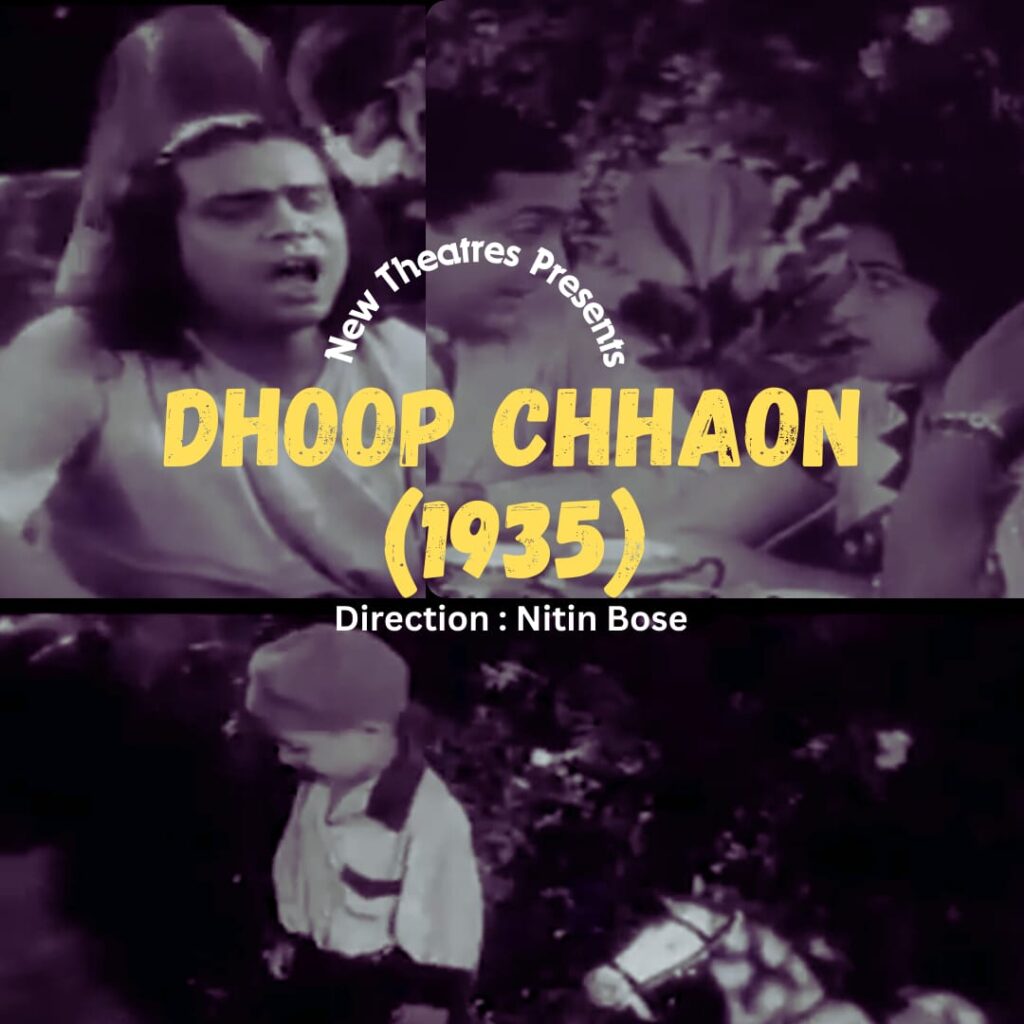अछूत कन्या: जब पर्दे पर पहली बार प्यार और सामाजिक बेड़ियाँ टकराईं साथ ही हिंदी सिनेमा की पहली ऑन-स्क्रीन जोड़ी की शुरुआत हुई।  अशोक कुमर और देविका रानी
अशोक कुमर और देविका रानी
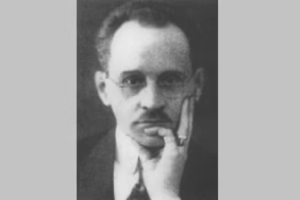 फ्रांज़ ओस्टेन (फिल्म निर्माता)
फ्रांज़ ओस्टेन (फिल्म निर्माता)
1936 में बॉम्बे टॉकीज के बैनर तले जर्मन निर्देशक फ्रांज़ ओस्टेन के निर्देशन में ‘अछूत कन्या‘ नामक एक फिल्म का निर्माण हुआ। बॉम्बे टॉकीज, जिसकी स्थापना 1934 में हिमांशु राय और देविका रानी ने की थी, हिंदी सिनेमा का एक प्रतिष्ठित स्टूडियो रहा है, जहां लगभग 40 फिल्मों का निर्माण किया गया।अछूत कन्या सामाजिक विषयों पर आधारित एक महत्वपूर्ण फिल्म थी, जिसकी कहानी समाज की छुआछूत जैसी कुरीति पर केंद्रित थी। फिल्म का शीर्षक — अछूत (Untouchable) और कन्या (Unmarried Girl) — इसके कथानक की मूल भावना को दर्शाता है।इस फिल्म में हिंदी सिनेमा की पहली लोकप्रिय ऑन-स्क्रीन जोड़ी, अशोक कुमार और देविका रानी, ने अभिनय किया। यह फिल्म अशोक कुमार की डेब्यू फिल्म भी थी, जिससे उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत की।
फिल्म की कहानी
अछूत कन्या :
ये फिल्म दो दोस्तों – दुखिया ( अछूत , रेलवे में फाटक का कर्मचारी ) और मोहनलाल ( ब्राह्मण , वैद्य और दुकानदार ) – की कहानी है। एक बार मोहनलाल को एक सांप काट लेता है तब दुखिया आगे आकर उसकी मदद करता है और सारा ज़हर निकालकर उसकी जान बचा लेता है। तब से दोनों गहरे दोस्त बन जाते है। हालांकि समाज उनकी दोस्ती को स्वीकार नहीं करता , लेकिन मोहनलाल पर इसका असर नहीं होता।

समय के साथ – साथ उनके बच्चे भी इस दोस्ती को बरकरार रखते है। दुखिया की बेटी कस्तूरी और मोहनलाल का बेटा प्रताप दोनों अच्छे दोस्त होते है और बचपन में साथ- साथ खेलते – घूमते बड़े होते है।


जैसे – जैसे उनकी शादी की उम्र होने लगती है प्रताप की माँ को दोनों का ज्यादा मिलना – घुलना पसंद नहीं आता। खासकर जब प्रताप कस्तूरी के घर का खाना खाने लगता है, क्योंकि वो एक अछूत कन्या है। उधर गांव में अफवाह फैलती है कि प्रताप और कस्तूरी की शादी तय हो गई है। मोहनलाल का विरोधी बापूलाल, जो खुद असफल वैद्य है, इस मौके का फायदा उठाकर गांव वालों को भड़काता है।
कुछ समय बाद प्रताप की माँ अपने बेटे के लिए मीरा नाम की एक लड़की से रिश्ता तय कर देती है।

साथ ही लड़की वालो से दान – दहेज़ न लेने का फैसला करती है। पर मोहनलाल कहता है कि उसे दहेज चाहिए ताकि वो उस दहेज को दुखिया की बेटी की शादी में दे पाए। देखते – ही – देखते प्रताप की शादी हो जाती है।


उधर दुखिया बीमार पड़ जाता है, और मोहनलाल उसे अपने घर इलाज के लिए लाता है, जिससे गांव वाले नाराज़ होकर उस पर हमला कर देते हैं और उसका घर जला देते हैं। पर फिर भी वो दुखिया का ही साथ देता है।

इसी दौरान फाटक के नियम तोड़ने के जुर्म में दुखिया की रेलवे की नौकरी चली जाती है। और उसकी जगह मन्नू (दुखिया के पुराने दोस्त का बेटा) आ जाता है। दुखिया अपनी बेटी की शादी मन्नू से कर देता है, जो पहले से शादीशुदा होता है।बाद में उसकी पहली पत्नी कजरी वापस आ जाती है, लेकिन कस्तूरी को इससे ऐतराज़ नहीं होता।


फिर एक दिन मीरा और कजरी की साजिश से कस्तूरी मेले में अकेली छूट जाती है, जहां उसकी मुलाकात प्रताप से होती है और घर लौटते समय फाटक पर प्रताप और मन्नू की लड़ाई होती है, और घोड़ा-गाड़ी पटरी पर फंस जाती है। तभी सामने से ट्रेन आने पर कस्तूरी ट्रेन रोकने जाती है, जिससे सवारियों की जान बच जाती है, लेकिन वो खुद मारी जाती है। उसकी मौत के बाद गांव वाले उसे अछूत से देवी का दर्जा दे देते हैं।



महिलाओं की भूमिका
इस फिल्म की कहानी में परंपरागत रूप से पुरुष और महिलाओं के कामों का विभाजन दिखाया गया है—जहां घरेलू कार्यों की ज़िम्मेदारी महिलाओं पर है और बाहरी कार्य पुरुषों के हिस्से में आते हैं।

हालांकि, फिल्म सामाजिक कुरीतियों जैसे दहेज प्रथा पर भी सवाल उठाती है, लेकिन एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ। फिल्म का एक प्रभावशील दृश्य तब सामने आता है जब प्रताप की माँ लेन-देन की बात पर साफ़ मना कर देती हैं और कहती हैं, “कुछ नहीं चाहिए, बेटे का ब्याह कर रही हूँ, कोई सौदा थोड़ी कर रही हूँ।” ये संवाद दहेज प्रथा के खिलाफ एक मजबूत संदेश देता है।
वहीं, कजरी का किरदार महिलाओं की स्वतंत्र सोच और आत्मनिर्णय की मिसाल बनकर उभरता है। वो अपने ससुराल वापस लौटने के लिए मायकेवालों का विरोध करती है। ये इस बात का प्रतीक है कि अगर व्यक्ति सही है और सामने वाला गलत, तो आवाज़ उठाने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए।
कजरी आर्थिक रूप से सशक्त है, जबकि उसका ससुराल उसकी तुलना में गरीब है, जिससे उसे मायके में रोकने की कोशिश की जाती है। जब उसे सही-गलत की पहचान होती है, तो वो वापस ससुराल जाने का निर्णय लेती है। इस पर उसकी दादी तंज कसती है —“बिलात भर की छोकरी और गज भर की जीभ” ये पुरानी सोच का प्रतिनिधित्व करता है, जो ये मानती है कि लड़कियों को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, खासकर जब वे अपने हक की बात करें। फिल्म इस दकियानूसी सोच को चुनौती देती है और महिलाओं की आवाज़ को सशक्त रूप से प्रस्तुत करती है।
वहीं दूसरी ओर, कहानी में दिखाया गया है कि एक पुरुष अपनी पत्नी की जानकारी और सहमति के बिना दूसरी शादी कर लेता है, आगे चलकर तीनो लोगो की ज़िंदगी उलझ जाती है। इसके बावजूद, पति को देवता और मालिक का दर्जा दिया जाता है। ये दो ऐसे शब्द है जो किसी को पूज्य या अपने अधीन बनाने का संकेत देते हैं, और ये धारणाएं कहीं – न – कहीं समाज में महिलाओं के अधिकारों का हनन दर्शाते हैं / करता है । फिर भी, फिल्म का संदेश महिलाओं को सम्मान और समानता देने का है। यह दर्शकों को एक बेहतर और प्रगतिशील सोच अपनाने के लिए प्रेरित करती है, जो समाज में लैंगिक समानता(Gender Equality) की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।
फिल्म एनालिसिस
फिल्म की पिक्चर क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, कुछ दृश्यों में कलाकारों के भाव-प्रदर्शन में कमी महसूस हुई। इसके बावजूद भी फिल्म की कहानी ने निराश नहीं किया, बल्कि अपने सामाजिक संदेश के साथ गहरी छाप छोड़ी। ब्रिटिश भारत के दौर के परिवेश पर आधारित इस फिल्म की पृष्ठभूमि उस दौर के सामाजिक ढांचे को उजागर करती है, जहां जाति व्यवस्था गहराई से जमी हुई थी। ब्राह्मण और अछूत जातियों के बीच के अंतर को फिल्म में बार-बार “अछूत” शब्द के प्रयोग के माध्यम से दर्शाया गया है, जो समाज में मौजूद गहरे भेदभाव को दर्शाता है।
कहानी दो पहलुओं पर केंद्रित है—एक ओर दो बच्चों की गहरी दोस्ती, जो एक-दूसरे के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हैं, और दूसरी ओर वही दो बच्चे बड़े होकर एक-दूसरे से प्रेम तो करते हैं, लेकिन विवाह की अनुमति उन्हें नहीं मिलती, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे विभिन्न जातियों से ताल्लुक रखते हैं।
प्रताप और कस्तूरी का एक-दूसरे के घर आना-जाना और साथ समय बिताना समाज को नहीं खटकता, लेकिन साथ भोजन करना और विवाह करना सही नहीं माना जाता , क्योंकि प्रताप ब्राह्मण है और कस्तूरी एक अछूत। फिल्म का एक भावुक दृश्य तब सामने आता है जब कस्तूरी अपने पिता से कहती है, “जब बचपन में साथ खेलना बुरा नहीं था, तो अब कैसे हो गया?”
हालाँकि प्रताप के पिता शुरुआत में इस रिश्ते के पक्ष में होते हैं, लेकिन पत्नी के समझाने पर वो भी अपना निर्णय बदल लेते हैं। अंततः सामाजिक दबाव के कारण दोनों अपने-अपने घरवालों की इच्छानुसार दूसरी जगह विवाह कर लेते हैं, और भले ही वे इस निर्णय से नाखुश है फिर भी खुश होकर अपने – अपने संबंधों को निभाते हैं।
ये फिल्म दिखाती है कि किस प्रकार समाज की सही -गलत धारणाएँ जैसे जाति, परंपरा और सामाजिक स्वीकृति, दो निर्दोष लोगो की मासूम दोस्ती और प्रेम को कुचल देती हैं। 1936 में रिलीज़ हुई ये फिल्म, न केवल जाति व्यवस्था पर एक साहसिक टिप्पणी प्रस्तुत करती है, बल्कि उस दौर में एक लड़का और एक लड़की की मित्रता को लेकर समाज के मानदंडों को भी उजागर करती है। ये अपने समय की सबसे चर्चित और सफल फिल्मों में से एक रही, जिसने सामाजिक मुद्दों को संवेदनशीलता और प्रभावशीलता के साथ बड़े पर्दे पर प्रस्तुत किया
यह फिल्म न सिर्फ़ एक प्रेम कहानी है, बल्कि समाज के आईने में झाँकने की एक कोशिश है—जहाँ प्यार तो जन्म से होता है, लेकिन शादी जाति देखकर होती है।
**क्या वाकई इंसानों के बीच रिश्तों की बुनियाद उनकी जाति होनी चाहिए, इंसानियत नहीं ?**